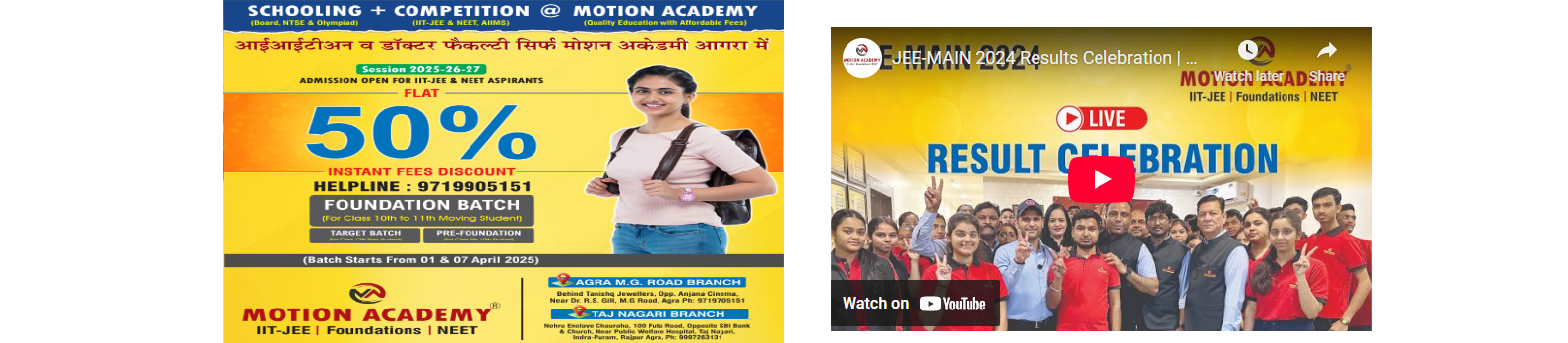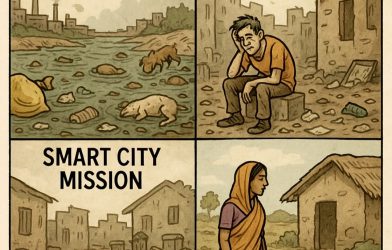पिछलग्गू बनकर चलना हित में नहीं, भारत को अब अपनी कूटनीति का पुनरीक्षण करना चाहिए, शक्ति पहचानना समय की मांग है
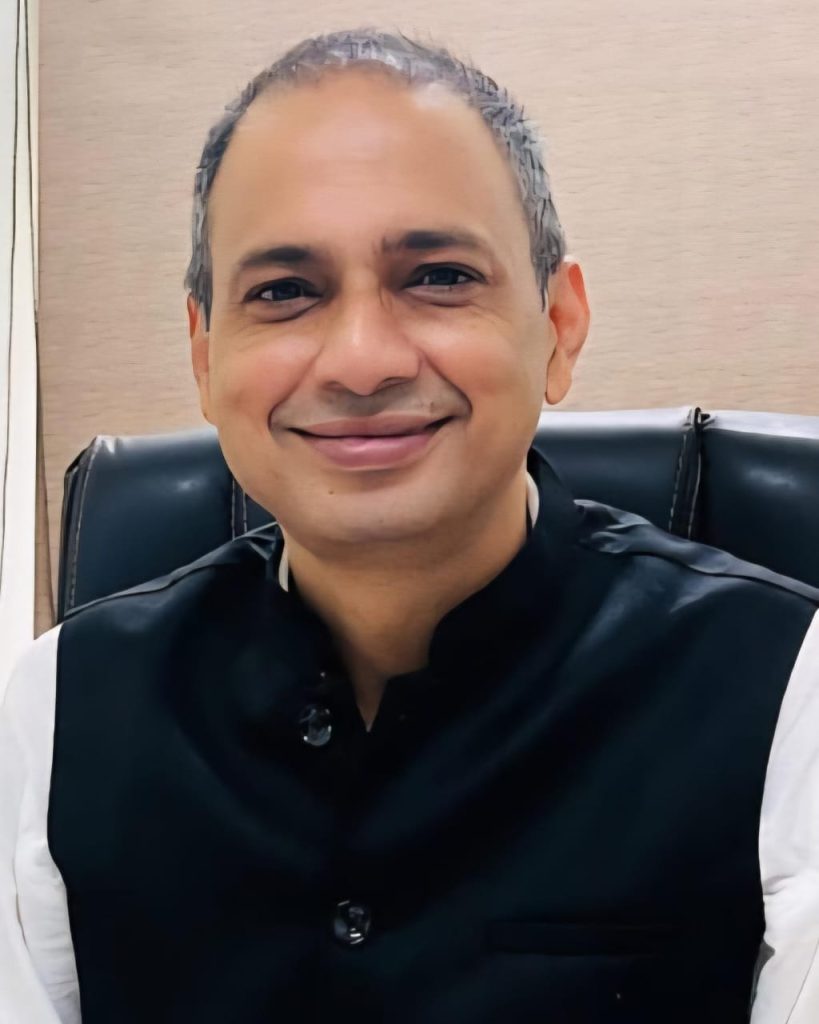
आज की वैश्विक राजनीति किसी भी प्रकार के आदर्शवाद या भावनात्मक मूल्यों से नहीं संचालित होती। कूटनीति अब नैतिक दावों का नहीं, हितों का विज्ञान बन चुकी है। युद्ध की विभीषिका हो या शांति सम्मेलन की मुस्कान, हर निर्णय के पीछे कोई न कोई रणनीतिक गणना, आर्थिक समीकरण या सैन्य लाभ छिपा होता है।
बीते दो दशकों में विश्व ने अनेक संकट देखे हैं, इराक पर आक्रमण, अफगानिस्तान से सैन्य वापसी, सीरिया में हस्तक्षेप, यूक्रेन संघर्ष और फिलिस्तीन-गाजा युद्ध। इन सभी घटनाओं में सार्वजनिक रूप से भले ही लोकतंत्र, मानवाधिकार और न्याय की बातें की गईं, किंतु निर्णयों के पीछे जो वास्तविक शक्तियाँ थीं, वे थीं राष्ट्रों के व्यापारिक हित, भू-राजनीतिक आकांक्षाएं और रक्षा उद्योग की अनवरत भूख। कूटनीति के इस यथार्थ में हथियार अब केवल युद्ध के उपकरण नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक पूर्ण राजनयिक मुद्रा बन चुके हैं। हथियारों की बिक्री और आपूर्ति वैश्विक संबंधों की दिशा निर्धारित करती है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी जैसे देश वर्षों से इस व्यापार को नियंत्रित कर रहे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक हथियार व्यापार में लगभग 77 प्रतिशत हिस्सा केवल इन पांच देशों के पास है। यह महज आंकड़ा नहीं, बल्कि एक राजनयिक वर्चस्व का प्रमाण है।
जब कोई देश किसी अन्य को हथियार बेचता है, तो वह केवल सौदा नहीं करता, वह एक दीर्घकालिक राजनीतिक और रणनीतिक रिश्ता गढ़ता है। हथियारों के ज़रिये केवल रक्षा क्षमता नहीं, बल्कि प्रभाव, निर्भरता और नियंत्रण भी स्थानांतरित होता है। यह संबंध अक्सर आर्थिक सहयोग से भी गहरा होता है और कई बार कूटनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने लगता है। यूक्रेन को दी जा रही सैन्य सहायता, या एस-400 जैसी प्रणालियों की आपूर्ति इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। भारत इस वैश्विक संतुलन का एक प्रमुख भागीदार है। वह विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और उसकी रक्षा ज़रूरतों का अधिकांश भाग रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों से पूरा होता है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच भारत के कुल रक्षा आयात में रूस का हिस्सा 36 प्रतिशत, फ्रांस का 17 प्रतिशत और अमेरिका का लगभग 11 प्रतिशत रहा। ऐसे परिदृश्य में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह किसी एक ध्रुव पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखे।
इस जटिल परिप्रेक्ष्य में भारत को एक संतुलित, व्यावसायिक और दूरदर्शी कूटनीति अपनानी होगी। उसे रक्षा आयात में विविधता लाते हुए घरेलू रक्षा उद्योग को सशक्त बनाना होगा। ‘मेक इन इंडिया’ केवल एक नारा न रह जाए, इसके लिए सरकारी निवेश, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निर्यात-नीति में सुधार आवश्यक हैं। भारत को यह समझना होगा कि कूटनीतिक स्वतंत्रता केवल बयानबाज़ी से नहीं, बल्कि विकल्पों की मौजूदगी से आती है। आज के दौर में राष्ट्र वही प्रभावी बन सकता है जो अपने निर्णयों को स्वायत्तता, सामर्थ्य और समझदारी के साथ ले। यह युग बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का है, जिसमें कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं, केवल स्थायी हित होते हैं। हथियार, तकनीक, ऊर्जा और बाजार ही अब नए शक्ति-स्रोत हैं।
ऐसे समय में भारत को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और विकल्पों से संचालित विदेश नीति की आवश्यकता है। एक ऐसी नीति, जो स्वदेशी क्षमता के साथ वैश्विक संतुलन भी साधे। तभी भारत वैश्विक मंच पर एक निर्णायक और आत्मनिर्भर शक्ति के रूप में उभर सकेगा।
(लेखक शिक्षाविद हैं।)